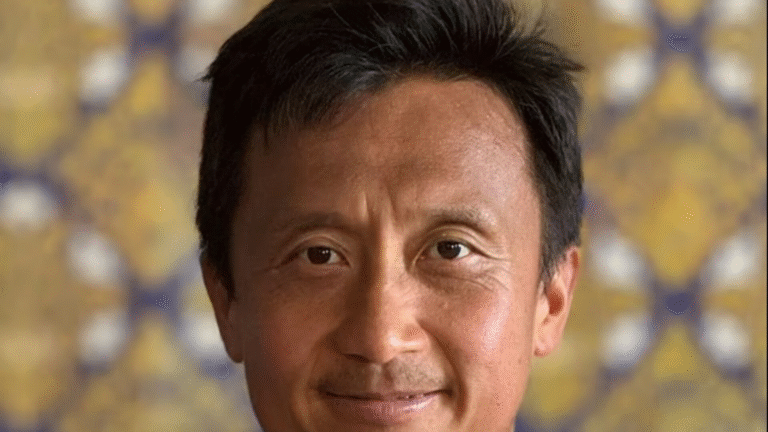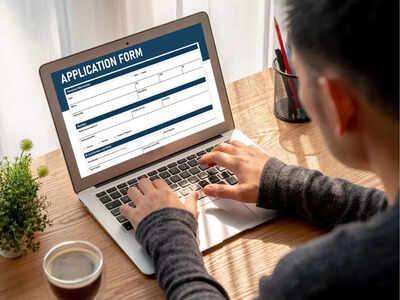ज़ेरोधा के सह-संस्थापक नितिन कामथ बताते हैं कि फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म ने भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में सहायता की है, फिर भी डिजिटल ऑनबोर्डिंग की चुनौतियाँ जारी हैं। वह उपयोगकर्ता-केंद्रित प्रौद्योगिकी डिजाइनों की वकालत करते हैं जो सीमाओं को संबोधित करते हैं और व्यवधान पैदा किए बिना कमजोर समुदायों का समर्थन करते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, कामथ कहा, “ज़ेरोधा सहित संपूर्ण भारतीय वित्तीय सेवा उद्योग, आधार ई-साइन, ईकेवाईसी आदि के माध्यम से डिजिटल ऑनबोर्डिंग में आसानी का एक बड़ा लाभार्थी रहा है। यह देश के टियर 2 और 3 शहरों और ग्रामीण हिस्सों में वित्तीय समावेशन में वृद्धि का एक बड़ा कारण रहा है; जिन लोगों ने पहले औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ बातचीत नहीं की थी।”
डिजिटल सिस्टम के सामने आने वाली समस्याएं
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, कामथ ने कहा, “हालांकि हम में से कई लोग इन डिजिटल प्रणालियों के लाभों को हल्के में लेते हैं, जैसे शहर में रहते हुए बेंगलुरु (और विशेषाधिकार की स्थिति), मैं ओटीपी सत्यापन और भौतिक/बॉयोमीट्रिक पक्ष के साथ चुनौतियों की सीमा से आश्चर्यचकित था।
के अनुसार कामथडिजिटलीकरण ने धोखाधड़ी और बर्बादी को कम किया है, लेकिन कोई भी प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन दोषरहित नहीं है।
“हालांकि डिजिटलीकरण ने धोखाधड़ी, रिसाव और बर्बादी को कम करने में मदद की है, लेकिन प्रौद्योगिकी का कोई भी कार्यान्वयन सही नहीं हो सकता है। सेबीउदाहरण के लिए, सख्त नियम हैं जो ब्रोकरों को एक ऐप जैसे केवल एक इंटरफ़ेस के बजाय कई मोड के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं, ”उन्होंने कहा।
उन्होंने आगे कहा, “बॉयोमीट्रिक उपकरण, विशेष रूप से, आदर्श परिस्थितियों में भी, कभी-कभी अपेक्षानुसार काम नहीं करते हैं। दूसरी चुनौती ओटीपी को लेकर है। भारत के दूरदराज के हिस्सों में लोग अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं, जिससे सत्यापन और लाभों के वितरण में देरी होती है। ये तकनीकी प्रणालियाँ गरीबों और कमज़ोर लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं।”
कामथ आगे उल्लेख किया गया कि प्रौद्योगिकी में व्यापार-बंद है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहां आर्थिक रूप से कमजोर आबादी रहती है। लाभ और हानि को संतुलित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चल रहे वित्तीय समावेशन प्रयासों के बीच मामूली व्यवधान भी दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
क्या किया जाए?
उन्होंने प्रथम-सिद्धांत, “ग्रेसफुल डिग्रेडेशन” दृष्टिकोण का उपयोग करके उपयोगकर्ता-केंद्रित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की वकालत की। नागरिक सेवाओं के लिए डिज़ाइन की गई सार्वजनिक प्रौद्योगिकी के मामले में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों की सीमाओं को पहचानना और सावधानीपूर्वक उन विकल्पों की योजना बनाना आवश्यक है जो व्यवधानों को कम करते हैं और इन डिजिटल प्रणालियों द्वारा सभी भारतीयों को प्रदान किए गए कड़ी मेहनत से प्राप्त लाभों को संरक्षित करते हैं।
नेटीजन क्या कहते हैं?
कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कामथ की पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिनमें से अधिकांश उनकी भावना से सहमत हैं।
उपयोगकर्ताओं में से एक ने लिखा, “हम वादे – और जमीनी हकीकत को देखते हैं। डिजिटल ऑनबोर्डिंग ने पहुंच को बढ़ाया है, लेकिन ग्रामीण हिस्सों में, वास्तविकता बहुत अलग है: परतदार नेटवर्क, असफल बायोमेट्रिक्स, और अपारदर्शी कमियां लोगों को कतारों में वापस धकेल देती हैं। हमें पहले विफलता के लिए डिजाइन करना चाहिए: ऑफ़लाइन पथ, मानव सहायता और स्थानीय विश्वास।”
एक अन्य ने कहा, “सही कहा। डिजिटल ऑनबोर्डिंग वित्तीय समावेशन के लिए एक गेम-चेंजर रही है, लेकिन कमियों को स्वीकार करना और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन करना इसे वास्तव में प्रभावशाली बना देगा।”
एक उपयोगकर्ता ने कहा, “बिल्कुल सहमत! डिजिटल ऑनबोर्डिंग पहल ने वास्तव में भारत में वित्तीय पहुंच को बदल दिया है, जिससे टियर 2 और 3 शहरों में अपार संभावनाएं खुल गई हैं। ऐसी प्रगति देखना रोमांचक है।”